बिहार विधानसभा चुनाव 2025: कौन कितनी बार बना सीएम और कितनी बार लगा राष्ट्रपति शासन? जानें सबकुछ
punjabkesari.in Tuesday, Oct 07, 2025 - 06:57 PM (IST)

नेशनल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और आरजेडी-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच है। वर्ष 1952 में बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। तब से लेकर 2020 तक कुल 17 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि अब तक चुनावों का इतिहास क्या रहा, किस पार्टी ने कितनी बार जीत हासिल की और राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
2020 विधानसभा चुनाव
2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लड़ा। एनडीए में इन दोनों दलों के अलावा जीतराम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी भी शामिल थी। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल-सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम शामिल थे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया। बीजेपी ने 74, जेडीयू 43 और कांग्रेस 19 सीटें जीती। एलजेपी एक सीट जीत पाई। एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।
2015 विधानसभा चुनाव
2015 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में पांच चरणों में हुआ। मुख्य मुकाबला महागठबंधन (जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस) और एनडीए (भाजपा और सहयोगी) के बीच था। महागठबंधन को कुल 178 सीटों पर जीत मिली जबकि एनडीए केवल 58 सीटों पर सिमट गई। जनता दल (यूनाइटेड)-71, राष्ट्रीय जनता दल-80 और कांग्रेस-27 सीटों पर विजयी रही। एनडीए में भाजपा-53, लोजपा-2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा-1 सीट हासिल कर सकी। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

2010 विधानसभा चुनाव
2010 में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन था। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़ी पार्टी बनी। जेडीयू ने 141 सीटों में से 115 और बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं। राष्ट्रीय जनता दल ने 168 सीटों में से केवल 22 सीटें जीतीं। कांग्रेस को केवल 4 सीटों पर सफलता मिली। इस चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।
2005 विधानसभा चुनाव
2005 में दो बार चुनाव हुए। फरवरी में आरजेडी को 75, जेडीयू को 55 और बीजेपी को 37 सीटें मिलीं। कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। अक्टूबर-नवंबर में जेडीयू 88, बीजेपी 55, आरजेडी 54, लोजपा 10 और कांग्रेस 9 सीटें जीत सकी। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई।
2000 बिहार विधानसभा चुनाव
1997 में राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव था। यह वह दौर था जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का निर्माण नहीं हुआ था। साल 2000 के नवंबर में झारखंड का गठन हुआ। उस समय बिहार में कुल 324 विधानसभा सीटें थीं और सरकार बनाने के लिए बहुमत यानी 162 सीटों की आवश्यकता थी।
इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कुल 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और 124 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं, भाजपा ने 168 में से 67 सीटें जीती। नीतीश कुमार की पार्टी को 120 में से 34 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस केवल 23 सीटों पर सफल रही। कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी फिर से बिहार की मुख्यमंत्री बनीं।

1995 बिहार विधानसभा चुनाव
1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में न तो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का उदय हुआ था और न ही जनता दल (यूनाइटेड) / JDU का। 1994 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से अलग होकर समता पार्टी का गठन किया था।
इस चुनाव में लालू प्रसाद की अगुवाई में जनता दल (JD) ने कुल 264 सीटों पर चुनाव लड़ा और 167 सीटों पर जीत हासिल की। भाजपा ने 315 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन केवल 41 सीटों पर ही सफलता मिली। कांग्रेस को केवल 29 सीटें ही मिल पाईं। इसके अलावा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 10 सीटें और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने 7 सीटें जीतीं। चुनाव के परिणामस्वरूप लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने।

1990 बिहार विधानसभा चुनाव
1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल (JD) ने पहली बार चुनाव लड़ा और 122 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। सरकार बनाने के लिए 162 सीटों का बहुमत आवश्यक था। इस चुनाव में कांग्रेस ने 71 सीटें, भाजपा 39 सीटें, जेएमएम 19 सीटें और CPI 23 सीटें जीतीं। बहुमत न होने के बावजूद, भाजपा और अन्य दलों के समर्थन से लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जनता दल ने बिहार में सरकार बनाई।
1985 बिहार विधानसभा चुनाव
1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे कुल 196 सीटें मिलीं, जो बहुमत से कहीं अधिक थीं। वहीं, लोकदल को 46 और भाजपा को 16 सीटें मिलीं। इस चुनाव के बाद बिहार में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली और एक ही कार्यकाल में चार मुख्यमंत्री बदले। 1985 से 1988 तक बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद भागवत झा आजाद लगभग एक साल तक मुख्यमंत्री बने। फिर सत्येंद्र नारायण सिंह और उसके बाद डॉ. जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार के मुख्यमंत्री पद संभाला।
1980 में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंदिरा) ने शानदार जीत दर्ज की और पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। इस चुनाव में कांग्रेस ने 324 सीटों में से 169 सीटें जीती। वहीं, जनता पार्टी (सेक्युलर) को 42, सीपीआई को 23, भाजपा को 21, जनता पार्टी को 13, इंडियन कांग्रेस यू-14, जेएमएम-11 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 23 सीटें मिलीं। यह चुनाव 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण वापसी साबित हुआ। चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जगन्नाथ मिश्र ने 8 जून 1980 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। इस चुनाव के बाद बनी सरकार ने अपना पूर्ण पाँच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया।
1977 बिहार विधानसभा चुनाव
1977 में बिहार में विधानसभा चुनाव मई-जून में आयोजित हुए। यह चुनाव आपातकाल (1975-77) के बाद हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी की लहर चली, जिसने केंद्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार को पराजित किया। बिहार में मुख्य मुकाबला जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के बीच था। चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें, कांग्रेस ने 57, सीपीआई ने 21, निर्दलीयों ने 24 और अन्य दलों ने 8 सीटें जीतीं। जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जो आपातकाल के खिलाफ जनता के गुस्से और पार्टी की एकजुटता का परिणाम था। चुनाव जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने 24 जून 1977 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके बाद रामसुंदर दास ने मुख्यमंत्री पद संभाला।
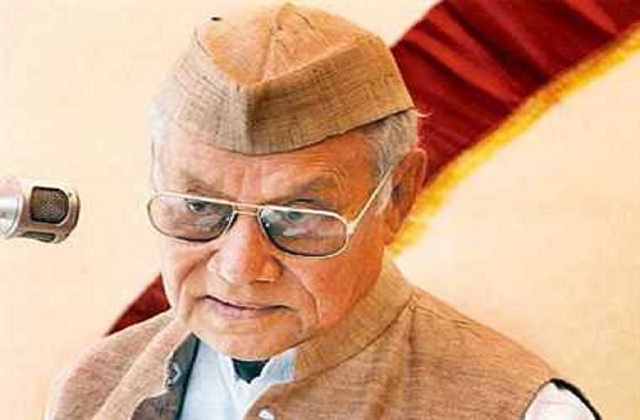
1972 बिहार विधानसभा चुनाव
1972 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की। कांग्रेस को कुल 167 सीटें हासिल हुईं, जबकि कांग्रेस (ओ) को 30 सीटों पर सफलता मिली। इसके अलावा, भारतीय जन संघ ने 25 और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 33 सीटें जीतीं। चुनाव के बाद लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लगा। इसके पश्चात केदार पांडे, अब्दुल गफ़ूर और जगन्नाथ मिश्र ने अलग-अलग समय पर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
1969 बिहार विधानसभा चुनाव
फरवरी 1969 में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 318 सीटों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। मुख्य मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), भारतीय जनसंघ (BJS), समाजवादी दलों और अन्य क्षेत्रीय दलों के बीच हुआ। कांग्रेस ने 118, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 52, जनसंघ 34, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 18, CPI 25, लोकतांत्रिक दल 22, निर्दलीयों ने 26 और अन्य दलों ने 23 सीटें जीतीं। चुनाव के बाद राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और कई नेताओं ने अल्पकालिक सरकारें बनाई। राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान शास्त्री ने कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला।
1967 बिहार विधानसभा चुनाव
फरवरी 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव चौथे आम चुनावों के साथ हुए। इस चुनाव में कुल 318 सीटों के लिए मतदान हुआ। राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव का दौर था, जहां कांग्रेस का दबदबा था, लेकिन गैर-कांग्रेसी दलों, विशेषकर समाजवादी दल और जनसंघ ने भी मजबूत चुनौती पेश की।
1967 में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 128 सीटें मिलीं, लेकिन 318 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 160 सीटें कांग्रेस के पास नहीं थीं। अन्य दलों ने भी सफलता पाई: संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (SSP)-68, भारतीय जनसंघ (BJS)-26, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP)-18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)-24, स्वतंत्र पार्टी-6, निर्दलीय-37 और अन्य पार्टियां-11 सीटें जीत सकीं।
कांग्रेस को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण गठबंधन और अस्थिरता का दौर शुरू हुआ। इस स्थिति में महामाया प्रसाद सिन्हा (जन क्रांति दल, बाद में कांग्रेस में शामिल) ने 5 मार्च 1967 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनकी सरकार संयुक्त मोर्चा (संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और अन्य दलों के समर्थन) पर आधारित थी। हालांकि, यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी और 25 जनवरी 1968 को गिर गई।
इसके बाद सत्येंद्र नारायण सिन्हा (कांग्रेस) ने 1968 में कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद भोला पासवान शास्त्री (कांग्रेस) ने 22 मार्च 1968 को मुख्यमंत्री पद संभाला, और वे 29 जून 1968 तक इस पद पर रहे।
1962 विधानसभा चुनाव
1962 में बिहार विधानसभा चुनाव फरवरी में संपन्न हुए। उस समय बिहार में कुल 318 विधानसभा सीटें थीं। यह चुनाव भारत के तीसरे आम चुनावों के साथ हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने राज्य में मजबूत पकड़ बनाए रखी। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और अन्य दलों जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (PSP), स्वतंत्र पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के बीच रहा।

चुनाव परिणाम में कांग्रेस-185, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी-29, स्वतंत्र पार्टी-50, CPI-12, जनसंघ (BJS)-3, सोशलिस्ट पार्टी-7, निर्दलीय-24 और अन्य-8 सीटें जीतने में सफल रहे। चुनाव जीतने के बाद बिनोदानंद झा (INC) ने 25 फरवरी 1962 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 तक रहा, इसके बाद कृष्ण बल्लभ सहाय (INC) मुख्यमंत्री बने।
1957 विधानसभा चुनाव
1957 के बिहार विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च में हुए। उस समय कुल 318 सीटें थीं। चुनाव भारत के दूसरे आम चुनावों के साथ हुआ और कांग्रेस (INC) ने राज्य में मजबूत बहुमत हासिल किया। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, CPI, जनसंघ (BJS) के बीच रहा।
चुनाव परिणाम में कांग्रेस-210, PSP-31, CPI-7, BJS-4, झारखंड पार्टी-31, निर्दलीय-29 और अन्य-6 सीटें जीतने में सफल रहे। चुनाव जीतने के बाद श्रीकृष्ण सिंह (INC) मुख्यमंत्री बने। वे 1952 से पहले से ही मुख्यमंत्री पद पर थे और 1957 चुनाव के बाद भी इस पद पर बने रहे। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1961 तक चला, जब उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बिनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने। श्रीकृष्ण सिंह को "बिहार केसरी" के नाम से जाना जाता है।
1952 विधानसभा चुनाव
1952 बिहार विधानसभा चुनाव भारत के पहले आम चुनावों का हिस्सा था, जो मार्च-अप्रैल 1951/1952 में हुआ। उस समय बिहार में कुल 330 विधानसभा सीटें थीं। चुनाव में कांग्रेस (INC) का दबदबा था, लेकिन समाजवादी दल (SP), झारखंड पार्टी और अन्य छोटे दल भी सक्रिय थे।

चुनाव परिणाम में कांग्रेस-239, SP-23, झारखंड पार्टी-32, लोक सेवक संघ-7, CPI-2, निर्दलीय-24 और अन्य-3 सीटें जीतने में सफल रहे। चुनाव जीतने के बाद श्रीकृष्ण सिंह (INC) ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे 15 अगस्त 1947 से अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री थे और चुनाव के बाद भी इस पद पर बने रहे। उनका कार्यकाल 1952 से 1961 तक चला।











